तीन मोर्चों पर दलित चेतना की परीक्षा: संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई
भारत का लोकतंत्र आज अपने 75 वर्षों के इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ “राजनीतिक समानता” तो व्यापक हो चुकी है, पर “सामाजिक समानता” अब भी संघर्षशील है।
2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग 100 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, जिनमें करीब 16–17 करोड़ दलित मतदाता शामिल थे। ये मतदाता केवल संख्या नहीं हैं — ये उस ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक हैं, जो अछूत से नागरिक बनने तक का सफर तय कर चुकी है।
फिर भी, भारत के सामाजिक ढाँचे की एक कटु सच्चाई यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र ने सामाजिक न्याय को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी —
“हमने राजनीतिक समानता दी है, परंतु सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी हुई है। यदि हमने इसे समाप्त नहीं किया, तो वे असमानताएँ हमारी राजनीतिक व्यवस्था को उड़ा देंगी।”
आज वह चेतावनी प्रासंगिक लगती है।
2024 के बाद भारत में तीन ऐसी घटनाएँ घटीं, जो केवल समाचार नहीं थीं — वे सामाजिक संक्रमण की परीक्षा थीं।
ये घटनाएँ तीन अलग-अलग संस्थानों — न्यायपालिका, कार्यपालिका और समाज के जनस्तर — पर दलितों के साथ हुए अन्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इन तीनों मोर्चों पर एक नेता — राहुल गांधी — संविधान की आत्मा के पक्ष में खड़े दिखाई दिए।
पहला मोर्चा: न्यायपालिका — न्याय की कुर्सी पर जाति की छाया
सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, खुले कोर्ट में अपमान का शिकार बने। एक वकील ने उन पर जूता फेंका — यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि उस सामाजिक प्रतीक पर प्रहार था, जहाँ एक दलित न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा है।

न्यायमूर्ति गवई महाराष्ट्र के वर्धा जिले से आते हैं, जहाँ उनका परिवार बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से था। उन्होंने शिक्षा और संघर्ष के बल पर न्यायपालिका की सबसे ऊँची कुर्सी तक पहुँचना संभव किया। उनका वहाँ होना ही उस सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो संविधान ने वादा किया था।
पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के कथन और तर्कों में जो ज़हर था, वह इस बात का प्रमाण है कि जातिवादी मानसिकता अब भी जिंदा है। उसने अपने बचाव में धार्मिक कट्टरता और झूठे व्यक्तिगत किस्से जोड़े — जो न केवल असंगत थे, बल्कि समाज में घृणा फैलाने वाले थे।
चिंता की बात यह रही कि सरकार या शीर्ष नेताओं की ओर से इस अपमानजनक कृत्य की कोई ठोस निंदा नहीं हुई।
यह मौन केवल प्रशासनिक नहीं, वैचारिक भी था — मानो एक दलित न्यायाधीश पर हमला “सिस्टम की सहज प्रतिक्रिया” बन गया हो।
यह वही स्थिति है, जिसका उल्लेख अंबेडकर ने किया था — जब व्यक्ति ऊँचाई पर पहुँचता है, तो समाज उसे गिराने की कोशिश करता है।
दलित का “सत्ता में होना” आज भी बहुतों के लिए असहज है, क्योंकि वह सामाजिक पदानुक्रम को तोड़ता है।
यह घटना न्यायपालिका के भीतर समानता की नैतिक परीक्षा थी — और दुर्भाग्य से, वह परीक्षा असफल रही।
दूसरा मोर्चा: कार्यपालिका — ऊँचे पद पर भी अपमान की दीवार
हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे प्रशासनिक ढाँचे को झकझोर दिया।
उनके परिवार और सहयोगियों के अनुसार, वे अपने ही विभाग में निरंतर जातीय अपमान, मानसिक प्रताड़ना और अलगाव का शिकार थे। उन्होंने शिकायतें दर्ज कराईं, पर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।
आख़िरकार, एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने हार मान ली — यह आत्महत्या नहीं, बल्कि संस्थागत जातिवाद की हत्या थी।
भारत की नौकरशाही में यह कोई नई बात नहीं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्टें बार-बार कहती हैं कि सरकारी सेवाओं में पदोन्नति, पोस्टिंग और सामाजिक व्यवहार में SC/ST अधिकारियों को भेदभाव झेलना पड़ता है।
अभी भी कई मंत्रालयों में शीर्ष पदों पर उनकी उपस्थिति 5% से कम है।

पूरन कुमार की मौत इस बात की साक्षी है कि “सिस्टम के भीतर पहुँच जाना” बराबरी का संकेत नहीं होता।
यह उस ‘काँच की छत’ (glass ceiling) की तरह है, जहाँ एक दलित अधिकारी ऊपर तक देख सकता है, पर वहाँ पहुँचने पर उसे ‘अदृश्य अपमान’ का एहसास होता है।
डॉ. अंबेडकर ने कहा था —
“समानता कानून से नहीं, समाज की चेतना से आती है।”
कार्यपालिका में यह चेतना अभी भी अधूरी है।
पूरन कुमार की त्रासदी ने दिखा दिया कि सामाजिक समावेशन केवल नीति-पत्रों में है, व्यवहार में नहीं।
तीसरा मोर्चा: समाज का जनस्तर — गाँवों में दलित जीवन की नंगी सच्चाई
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हरि ओम वाल्मीकि नामक एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उसका अपराध केवल इतना था कि उसने ऊँची जाति के व्यक्ति का विरोध किया था।

यह घटना किसी अपवाद की तरह नहीं, बल्कि उस लंबी श्रृंखला का हिस्सा है जहाँ हर साल हज़ारों दलित केवल अपने अस्तित्व की कीमत चुका रहे हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 45,000 से अधिक अपराध अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज होते हैं, यानी हर घंटे पाँच से छह घटनाएँ।
पर दर्ज न होने वाली घटनाएँ इस आँकड़े से कहीं ज़्यादा हैं।
जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरि ओम के परिवार से मिलने पहुँचे, तो पुलिस ने उन्हें गाँव के बाहर रोक दिया।
यह दृश्य प्रतीकात्मक था — जैसे सत्ता और प्रशासन मिलकर दलित पीड़ा को ढँक देना चाहते हों।
दलितों के पक्ष में उठने वाली हर आवाज़ को “राजनीति” कहकर खारिज कर देना सत्ता की नई रणनीति बन गई है।
यहाँ सवाल यह नहीं है कि अपराधी कौन थे, बल्कि यह है कि राज्य किसके पक्ष में खड़ा था।
अगर पुलिस पीड़ित परिवार से मिलने वाले नेता को रोकती है, तो यह कानून नहीं, व्यवस्था की जातिवादी मानसिकता है।
हरि ओम वाल्मीकि की मौत भारत के गाँवों में दलित अस्तित्व की स्थायी त्रासदी है — जहाँ इंसान पहले जाति से पहचाना जाता है, नागरिकता से नहीं।
राहुल गांधी की भूमिका: संवैधानिक प्रतिरोध का नया विमर्श
इन तीनों मोर्चों पर राहुल गांधी की उपस्थिति केवल राजनीतिक नहीं थी — यह एक वैचारिक हस्तक्षेप था।
उन्होंने तीनों घटनाओं में संविधान की आत्मा को केंद्र में रखा और दलित प्रश्न को केवल “वोट बैंक” नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया।
1. विचारधारा का पुनर्पाठ
राहुल गांधी ने अपनी “भारत जोड़ो यात्रा” और “संविधान बचाओ” अभियानों के दौरान बार-बार कहा कि यह लड़ाई दो विचारों की है —
एक, जो बराबरी में विश्वास करती है (संविधान),
और दूसरी, जो मनुस्मृति की सामाजिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहती है।
उन्होंने कहा था —
“भारत में मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई अब भी जारी है; और हर नागरिक को तय करना है कि वह किसके साथ है।”
यह कथन केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि अंबेडकरवादी दृष्टिकोण का पुनरुत्थान है।
2. दलित चेतना को राष्ट्रीय विमर्श में लाना
पिछले दशक में दलित मुद्दे मीडिया और संसद दोनों से लगभग गायब हो गए थे।
राहुल गांधी का लगातार इन मामलों में सक्रिय रहना (भीमा-कोरेगांव, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सर्वोच्च न्यायालय की घटना पर टिप्पणी) इस बात का संकेत है कि वे दलित प्रश्न को मुख्यधारा राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते हैं।
वे डॉ. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार की परंपरा को पुनः जनचेतना में लाना चाहते हैं — जहाँ दलित अस्मिता केवल आरक्षण या सामाजिक कल्याण नहीं, बल्कि स्वाभिमान और न्याय की अवधारणा है।
3. सत्ताधारी विमर्श को चुनौती
सत्तारूढ़ दल जब “सबका साथ-सबका विकास” की बात करता है, तो वह सामाजिक बराबरी की जगह आर्थिक लाभ पर ज़ोर देता है।
पर राहुल गांधी का दृष्टिकोण इसे पलट देता है —
वे कहते हैं, विकास तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान सुनिश्चित न हो।
उनकी यह राजनीति “करुणा” की नहीं, “प्रतिरोध” की राजनीति है — जो कहती है कि संविधान केवल पढ़ने की चीज़ नहीं, जीने की ज़िम्मेदारी है।
तीनों घटनाएँ: एक साझा रेखा
जब हम इन तीनों प्रकरणों को साथ रखकर देखते हैं —
1. CJI गवई पर जूता फेंकना,
2. पूरन कुमार की आत्महत्या,
3. हरि ओम वाल्मीकि की हत्या —
तो स्पष्ट दिखता है कि यह तीनों एक ही सामाजिक पैटर्न के अलग-अलग चेहरे हैं।
दलित चाहे न्याय की कुर्सी पर बैठे, पुलिस की वर्दी पहने या खेत में मजदूर हो — समाज उसे बराबरी से स्वीकार नहीं करता।
यह जातिवादी ढाँचे की स्थायित्व का प्रमाण है।
इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट है कि जाति केवल व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि संस्थागत और राजनीतिक संरचना का हिस्सा बन चुकी है।
जो व्यवस्था दलित को दबाए रखने में सहज महसूस करती है, वही उसे “विकास” का झूठा सपना भी दिखाती है।
निष्कर्ष: संविधान की आत्मा को बचाने की पुकार
भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है —
“हम, भारत के लोग, न्याय — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक — सुनिश्चित करेंगे।”
पर जब देश के सबसे वंचित तबके के साथ अन्याय होता है, तो यह केवल व्यक्ति पर हमला नहीं — बल्कि संविधान की आत्मा पर प्रहार होता है।
आज का सवाल यह नहीं कि कोई नेता किस पार्टी से है, बल्कि यह है कि क्या हम संविधान के साथ हैं या मनुस्मृति के साथ?
मनुस्मृति कहती है कि समाज जन्म से बँटा है;
संविधान कहता है कि हर नागरिक समान है।
यह वही संघर्ष है जो हर युग में नया रूप लेता है — कभी अदालत में, कभी थाने में, कभी गाँव के चौपाल में।
जब तक दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों को वास्तविक सम्मान नहीं मिलेगा, भारत की प्रगति अधूरी रहेगी।
और जब तक सत्ता-संरचनाएँ सामाजिक न्याय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगी, लोकतंत्र केवल दिखावा रहेगा।
राहुल गांधी की यह पहल इसी अधूरी यात्रा की याद दिलाती है
कि यह लड़ाई किसी जाति या नेता की नहीं, बल्कि संविधान की गरिमा की है।
“समानता की माँग करना कोई अपराध नहीं,
वह तो लोकतंत्र का पहला धर्म है।”
यह लेख किसी राजनीतिक दल की वकालत नहीं करता, बल्कि उस विचार की पक्षधरता करता है
जो कहता है —
भारत तभी महान होगा जब हर नागरिक समान होगा।

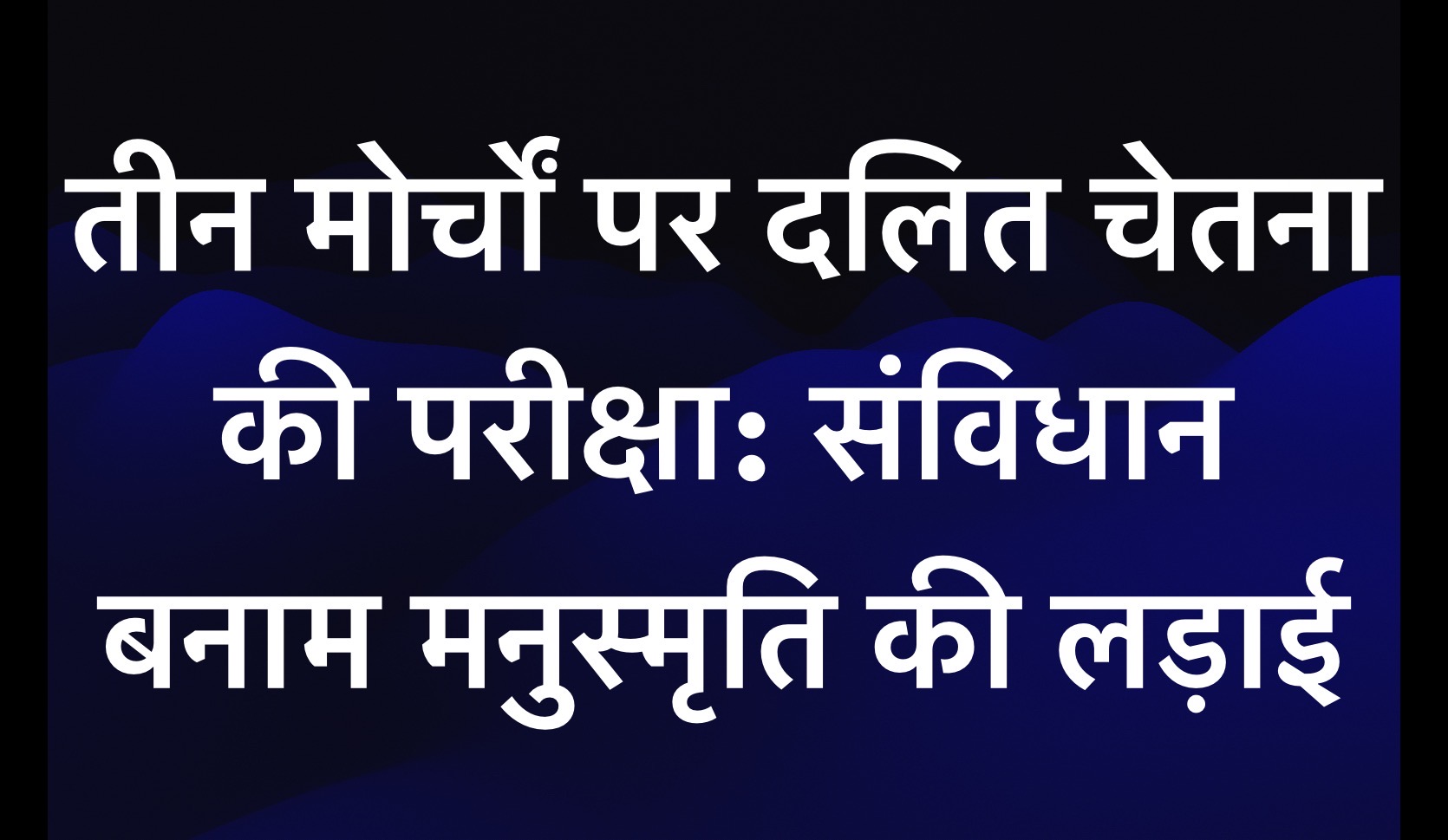
What resonated with me most was your point about the importance of small consistent actions. It’s easy to overlook how these tiny steps accumulate over time. Your personal story really brought this home in a way that statistics alone couldn’t.