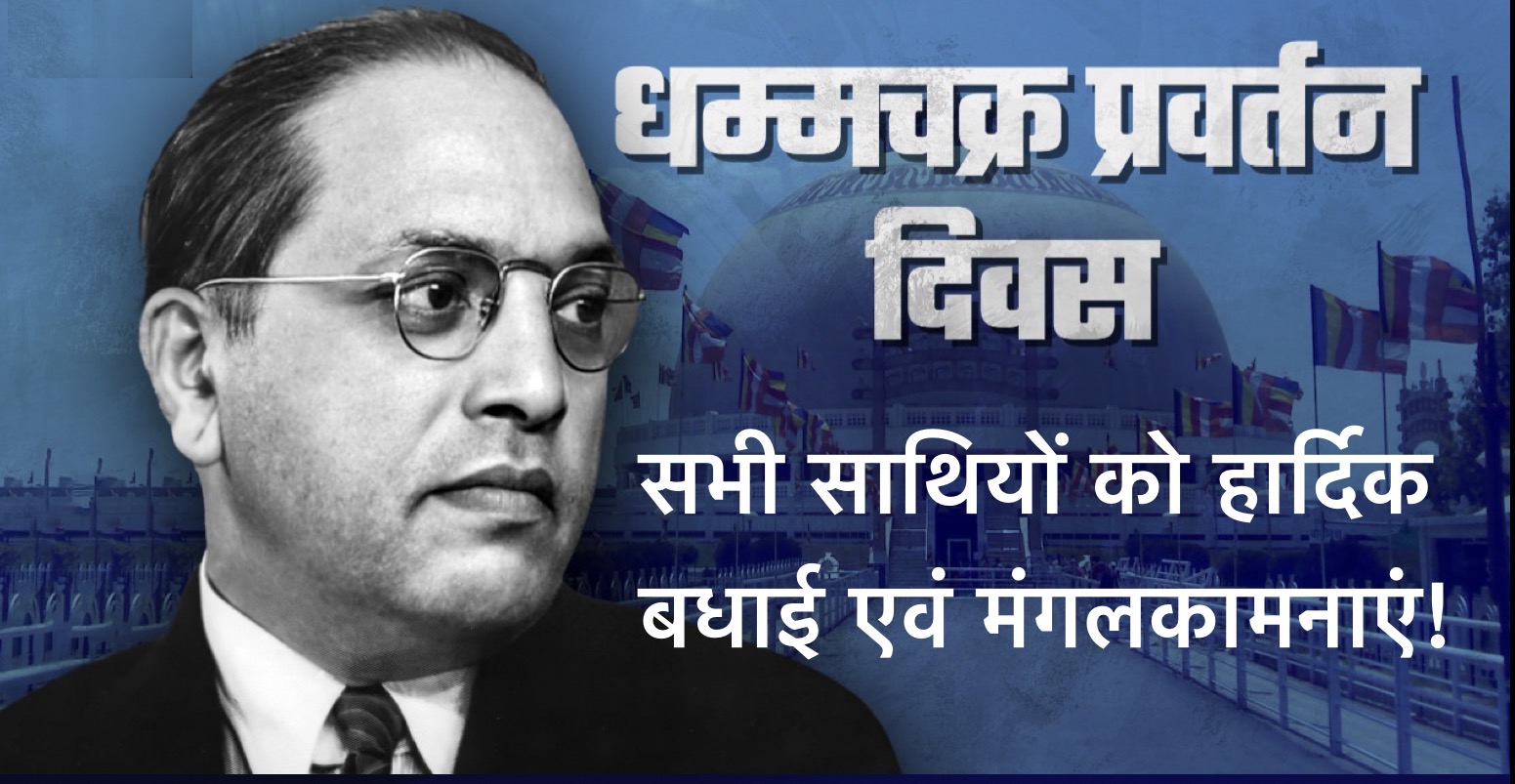धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस: बहुजन चेतना का पुनर्जन्म
1. ऐतिहासिक क्षण का अर्थ
14 अक्टूबर 1956 — यह वह दिन है जब नागपुर के दीक्षाभूमि पर लाखों बहुजन समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नेतृत्व में धम्म को पुनः अंगीकार किया।
यह केवल एक धार्मिक दीक्षा नहीं थी; यह एक मानव-मुक्ति आंदोलन की औपचारिक घोषणा थी।
इस दिन डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं बुद्ध, धम्म और संघ की त्रिरत्न शरण लेकर अपने अनुयायियों को जीवन का नया दर्शन दिया — “मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य बनकर रहूँगा।”
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इसीलिए केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्जन्म, आत्मसम्मान और प्रतिरोध की घोषणा का प्रतीक है।
2. बौद्ध दीक्षा का उद्देश्य: धर्मांतरण नहीं, मन परिवर्तन
डॉ. अम्बेडकर के लिए बौद्ध धर्म अपनाना किसी धार्मिक प्रतिस्थापन का साधन नहीं था। वे कहते थे—
“मैं धर्म इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने भाग्य को बदलना चाहता हूँ।”
उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म मनुवादी, जन्माधारित और असमानता पर टिका हुआ था। उन्होंने उस व्यवस्था को ठुकराकर एक ऐसे धर्म का चुनाव किया जिसमें समता, करुणा, प्रज्ञा और नैतिकता सर्वोपरि हो।
उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा—
“अब तुम हिन्दू नहीं, मनुष्य हो। तुम किसी के गुलाम नहीं, बुद्ध के अनुयायी हो।”
इस प्रकार, धम्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ था — शोषण के पहिये को रोकना और करुणा के चक्र को चलाना।
3. धम्म और आधुनिकता का संवाद
डॉ. अम्बेडकर का धम्म आधुनिक युग का धम्म था — तर्क, विज्ञान और मानवतावाद पर आधारित।
उन्होंने इसे “Navayana” — अर्थात् नया वाहन कहा, जो परंपरागत बौद्ध संप्रदायों से अलग था।
उनका धम्म न तो केवल ध्यान की साधना था, न ही संन्यास की परंपरा; वह था सामाजिक कर्मयोग और न्याय की साधना।
इस धम्म में करुणा और समानता के साथ-साथ संविधानिक मूल्य भी निहित हैं —
• समता: कोई ऊँच-नीच नहीं, हर व्यक्ति समान सम्मान का अधिकारी।
• स्वतंत्रता: किसी धर्मगुरु, जाति या परंपरा की दासता नहीं।
• बंधुता: समाज के सभी वर्गों में प्रेम, सहयोग और साझा जिम्मेदारी।
4. धम्मचक्र प्रवर्तन: बहुजन राजनीति का सांस्कृतिक आधार
कांशीराम और बहुजन आंदोलन ने डॉ. अम्बेडकर की इसी चेतना को राजनीतिक रूप दिया।
“धम्मचक्र प्रवर्तन” ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता परिवर्तन तभी टिकाऊ होगा जब समाज का सांस्कृतिक आधार बदलेगा।
कांशीराम ने कहा था —
“राजनीति शक्ति का स्रोत है, पर संस्कृति दिशा का निर्धारण करती है।”
बुद्ध, कबीर, फुले, पेरियार और अम्बेडकर — इन सबका साझा ध्येय यही था कि बहुजन समाज अपने इतिहास, विचार और जीवन के अर्थ को स्वयं परिभाषित करे।
आज जब बहुजन आंदोलन में बिखराव है, तब यह दिवस स्मरण कराता है कि सामाजिक जागृति के बिना राजनीतिक जागरण अधूरा है।
5. आज के भारत में धम्म की प्रासंगिकता
2025 के भारत में जाति, धर्म और पूँजी का गठजोड़ फिर से बहुजनों को हाशिए पर ढकेल रहा है।
• शिक्षा, रोजगार और न्याय में असमानता बढ़ रही है।
• मीडिया और राजनीति में मनुवादी विचारधारा का वर्चस्व स्पष्ट है।
• “शिक्षित करो, संगठित हो, संघर्ष करो” का संदेश पुनः उपेक्षित होता जा रहा है।
ऐसे में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी पुनःस्मरण है —
हमें याद दिलाने के लिए कि बुद्ध का मार्ग निष्क्रियता नहीं, जागरूक कर्म का मार्ग है।
आज आवश्यकता है —
• बुद्ध और अम्बेडकर के विचारों को शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय स्थान देने की।
• बहुजन युवाओं को “पे बैक टू सोसाइटी” के भाव से सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाने की।
• मीडिया और राजनीति में नव-बौद्ध नैतिकता का पुनर्पाठ करने की।
6. एकजुटता का धम्म
बुद्ध का धम्म कहता है — “संघं शरणं गच्छामि।”
संघ केवल धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि संगठित समाज का प्रतीक है।
डॉ. अम्बेडकर ने भी कहा था —
“जो समाज संगठित नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं रह सकता।”
आज बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है — संगठन।
जब तक जातिगत विभाजन और व्यक्तिगत स्वार्थ हावी रहेंगे, तब तक बहुजन चेतना अधूरी रहेगी।
संगठन ही वह धम्म है जो असंख्य ‘अकेले’ लोगों को एक समवेत शक्ति में बदल सकता है।
7. निष्कर्ष: धम्म ही मुक्ति का मार्ग
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मुक्ति कोई वरदान नहीं, एक सतत् संघर्ष है।
डॉ. अम्बेडकर ने जिस “धम्मराज्य” का स्वप्न देखा था, वह केवल धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक स्वतंत्रता का प्रतीक था।
आज हमें फिर वही प्रण दोहराना होगा —
“हम शोषण के नहीं, मानवता के अनुयायी हैं।
हम गुलामी के नहीं, समता के मार्ग पर चलेंगे।”
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प है —
एक ऐसे भारत के निर्माण का,
जहाँ हर मनुष्य समान अवसर, समान सम्मान और समान स्वप्न का अधिकारी हो।