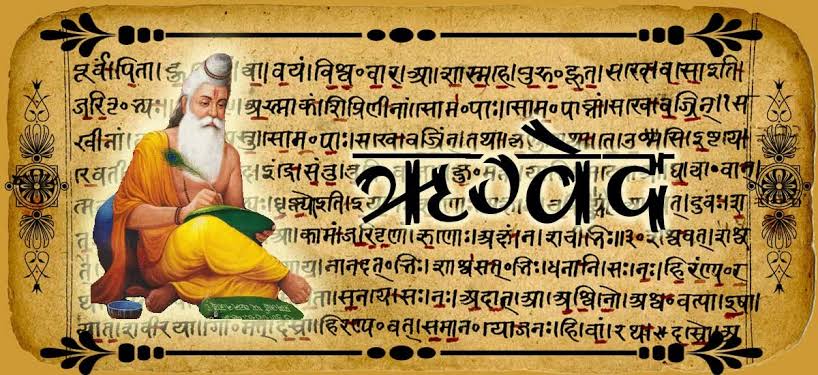वेदों की प्राचीनता: एक मिथक
वेदों का भौगोलिक साक्ष्य और मौखिक मिथक: एक आलोचनात्मक विश्लेषण
“वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं।” यह कथन भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में एक मौलिक और अटल सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। किंतु, जब इसकी ऐतिहासिकता की कसौटी पर इतिहास और पुरातत्व का प्रमाण-आधारित लेंस लगाया जाता है, तो यह दावा एक जटिल पहेली बनकर रह जाता है। यह आलेख इसी पहेली का विश्लेषण करता है और यह प्रश्न उठाता है: क्या वेदों की सर्वव्यापी प्राचीनता एक ऐतिहासिक तथ्य है, या फिर एक सुविधाजनक ‘मौखिक मिथक’ का परिणाम?
1. भारत के बाहर वेद: पुरातात्विक निर्वात
वैश्विक पुरातात्विक रिकॉर्ड में वेदों का कोई स्थान नहीं है। यह एक कठोर परंतु निर्विवाद सत्य है।
· शून्य पांडुलिपियाँ एवं अभिलेख:
मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, ईरान, मध्य एशिया या चीन जैसी सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यताओं से प्राप्त असंख्य अभिलेखों और पांडुलिपियों में वेदों के किसी मंत्र, सूक्त या ऋषि का उल्लेख नहीं मिलता। यदि वेद वास्तव में इतने सार्वभौमिक और प्राचीन थे, तो उनके वैश्विक प्रभाव के कम से कम कुछ निशान तो अवश्य मिलने चाहिए थे।
· अवेस्ता:
एक समानांतर, स्वतंत्र विकास: ईरानी धर्मग्रंथ ‘अवेस्ता’ और ऋग्वेद में भाषाई एवं पौराणिक समानताएँ हैं, जो एक सामान्य भारोपीय मूल की ओर इशारा करती हैं। किंतु यह समानता ‘पहचान’ नहीं है। अवेस्ता में वेदों का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। बल्कि, दोनों में मौलिक वैचारिक विरोधाभास हैं; जहाँ वेदों में ‘देव’ शुभ देवता हैं, अवेस्ता में उन्हें ‘दैव’ यानी दानव कहा गया है। यह स्पष्ट करता है कि अवेस्ता वेदों की एक शाखा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र सहोदर परंपरा है।
· मितानी सन्धि-लेख:
देवताओं के नाम, वेद नहीं: सी. 1400 ई.पू. की मितानी सभ्यता (सीरिया-तुर्की) की एक संधि में इंद्र, वरुण, मित्र जैसे देवताओं के नाम मिलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज है, परंतु यह सिद्ध नहीं करती कि ऋग्वेद उस समय और स्थान पर विद्यमान था। यह केवल यह इंगित करता है कि भारोपीय जनजातियाँ इन देवताओं की पूजा करती थीं। वेद नामक एक सुसंहत, संकलित ग्रंथ का कोई प्रमाण नहीं है।
निष्कर्ष:
भारत की सीमाओं के बाहर वेदों के अस्तित्व का कोई भौतिक या प्रत्यक्ष साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह निर्वात इस दावे पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है कि वेद एक वैश्विक या अति प्राचीन सभ्यता का आधारस्तंभ थे।
2. मौखिक परंपरा: विश्वास बनाम प्रमाण का विज्ञान
वेदों की प्राचीनता के पक्ष में प्रस्तुत किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली तर्क उनकी ‘श्रुति’ या मौखिक परंपरा है। कहा जाता है कि इन ग्रंथों को हजारों वर्षों तक अक्षरशः कंठस्थ करके सुरक्षित रखा गया। जबकि मौखिक परंपराएँ सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में उनकी सीमाएँ हैं।
· असत्यापनीयता:
मौखिक परंपरा का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसकी प्रामाणिकता और प्राचीनता को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता। कार्बन डेटिंग, लिपि विश्लेषण या पाठीय स्तरीकरण जैसी वैज्ञानिक पद्धतियाँ इसमें लागू नहीं होतीं। इस प्रकार, यह पूर्णतः ‘विश्वास’ के क्षेत्र में रहती है।
· एक सुविधाजनक ‘मिथक’:
मौखिक परंपरा का तर्क एक सुविधाजनक उपकरण बन गया है जिसके द्वारा ग्रंथों को ऐतिहासिक आलोचना और पुरातात्विक जाँच से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ग्रंथ को ‘अपौरुषेय’ (मानव-रचित नहीं) और ‘अनादि’ घोषित कर देने से उसके ऐतिहासिक संदर्भ और कालनिर्धारण का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। यह एक Post-facto (बाद में गढ़ा गया) औचित्य है जिसका उद्देश्य एक अप्रमाणित दावे को अतिप्राचीन बनाना है।
· वैश्विक संदर्भ में असंगति:
विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं (मिस्र, सुमेर, चीन) ने अपने महत्वपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक ग्रंथों को लिखित रूप में अभिलेखित किया। केवल भारत के संदर्भ में यह अवधारणा कि “हमारे ग्रंथ इतने पवित्र और प्राचीन थे कि उन्हें लिखा ही नहीं गया,” एक विलक्षण और संदेहास्पद अपवाद प्रतीत होती है।
3. भारत के भीतर साक्ष्य: एक विलंबित उद्भव
भारत के भीतर भी वेदों का लिखित साक्ष्य आश्चर्यजनक रूप से बहुत बाद का है।
· प्रारंभिक लिपि का अभाव:
सिंधु घाटी सभ्यता (c. 3300–1300 BCE) की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और उसमें वैदिक साहित्य का कोई संकेत नहीं मिलता है।
· सबसे पुरानी उपलब्ध पांडुलिपियाँ:
वेदों की सबसे पुरानी उपलब्ध पांडुलिपियाँ 11वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास की हैं, जो नेपाल से प्राप्त हुई हैं। यह ऋग्वेद के रचनाकाल के प्रस्तावित समय (c. 1500–1000 BCE) से लगभग 2000 वर्ष बाद की हैं। यह विशाल अंतराल स्वयं में एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
निष्कर्ष: प्राचीनता के मिथक का भंजन
इस आलोचनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि वेदों की सर्वव्यापी और अतिप्राचीन होने की अवधारणा एक ऐतिहासिक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक-वैचारिक निर्माण प्रतीत होती है।
1. भौगोलिक अलगाव:
वेदों का कोई अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य न होना दर्शाता है कि वे एक क्षेत्र-विशेष (भारतीय उपमहाद्वीप) की साहित्यिक-धार्मिक अभिव्यक्ति थे, न कि एक वैश्विक प्राचीन सभ्यता का आधार।
2. मौखिकता का रक्षा-कवच:
मौखिक परंपरा का तर्क एक सुरक्षा-कवच के रूप में कार्य करता है, जो इन ग्रंथों को ऐतिहासिक जाँच से बचाता है और उनकी प्राचीनता को एक ‘आस्था का विषय’ बनाकर उसे चुनौती से परे रखता है।
3. वास्तविक ऐतिहासिकता:
वेद निस्संदेह प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक और किंतु, उनकी ‘प्राचीनता’ को एक पौराणिक, अतिप्राकृतिक कालखंड में स्थापित करने के बजाय, एक ऐतिहासिक-भौगोलिक संदर्भ में समझना अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत होगा।